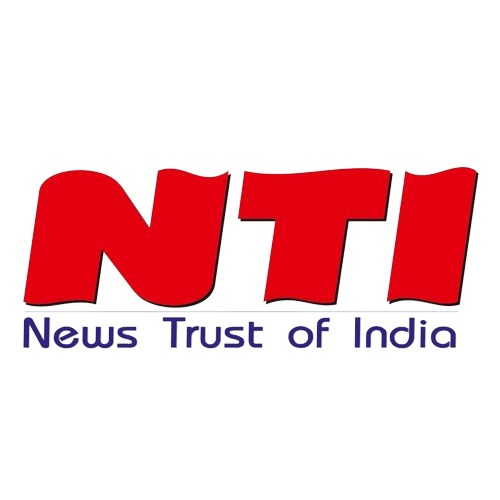NTI (मोहन भुलानी ) : हिमालय एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जो 2,500 किलोमीटर की लंबाई में कश्मीर से अरुणाचल तक फैली हुई है। यह 7,000-8,000 मीटर ऊंची चोटियों का एक विशाल नेटवर्क है, जो लाखों वर्षों से अपने आसपास के पर्यावरण और भूगोल पर गहरा प्रभाव डालता रहा है। यह प्रभाव उत्तर और दक्षिण दिशाओं में बिल्कुल भिन्न रूपों में दिखाई देता है। इस विशाल पर्वत शृंखला ने न सिर्फ प्रकृति को एक नया आकार दिया, बल्कि यहां बसे लोगों की संस्कृतियों को भी गढ़ा। हिमालय की यह ऊंची दीवार इन समुदायों को आपस में अलग करती रही, जिसके कारण उनकी संस्कृतियां अलग-अलग रास्तों पर विकसित हुईं। फिर भी, कुछ जातीय समूह ऐसे थे जो इन दो भिन्न दुनिया को जोड़ने वाली कड़ी बन गए।
ये लोग इस पहाड़ी भूलभुलैया में बसे थे, कुछ ऐसी घाटियों में जो रहने योग्य थीं। इनके जीवन का आधार व्यापार बन गया। हर साल ये लोग दक्षिणी क्षेत्रों से अनाज, बर्तन, गुड़ जैसी चीजें अपनी बकरियों और भेड़ों पर लादते थे और ऊंचे पहाड़ी दर्रों को पार कर तिब्बत तक जाते थे। वहां से वे नमक, ऊन, सोना और बोरेक्स लेकर दक्षिण की ओर लौटते थे। यह सिलसिला हर साल दोहराया जाता था। हिमालय की पूरी लंबाई में ऐसे अर्ध-खानाबदोश समूह फैले हुए थे। आज ये सभी एक सामान्य नाम से पहचाने जाते हैं, जो उनके दक्षिणी भाइयों ने दिया—भोटिया। हर भोटिया समूह की अपनी अलग बोली, संस्कृति और आत्म-पहचान है।
जोहार घाटी और शौका भोटिया
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की जोहार घाटी जो शौका भोटियाओं का घर है। “भोटिया” शब्द “भोट” से संबंधित किसी भी चीज को दर्शाता है। “भोट” तिब्बती शब्द “बोड” से आया है, जिसका अर्थ तिब्बत ही है। आमतौर पर जिन्हें हम “भोटिया” कहते हैं, वे “बोड” के दक्षिण में रहते हैं, खासकर उत्तराखंड में। यह शब्द अपने आप में एक प्रकार का गलत नाम है। फिर भी, उत्तराखंड में सात भोटिया समूह हैं, जो तिब्बत से सटी नदी घाटियों में रहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए: जाध लोग जाध गंगा की घाटी में रहते हैं; सरस्वती-अलकनंदा की घाटी में मरछा लोग माना के पास और तोलछा लोग धौली की घाटी में नीति-मलारी-गमशाली गांवों में रहते हैं; कुमाऊं में गोरी गंगा की घाटी में शौका जनजाति रहती है।
उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर रुंग भोटिया रहते हैं, जो तीन समूहों में बंटे हैं: दार्मी/दरमानिस (दरमा घाटी में), चौदांसी (चौदांस में), और ब्यांसी (ब्यांस में)। उत्तराखंड के सभी भोटिया मौसमी प्रवासी हैं। गर्मियों में वे अपने ऊपरी, उत्तरी गांवों में रहते थे, और सर्दियों में दक्षिणी, निचले गांवों में चले जाते थे। जोहार के शौका भी इस नियम से अलग नहीं थे। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि उत्तराखंड के भोटियाओं के विपरीत, हमारे पड़ोसी क्षेत्रों में यह प्रवासी जीवनशैली बहुत प्रचलित नहीं है।
पड़ोसियों से तुलना
इतिहासकार डॉ. शेखर पाठक के अनुसार, यह बहुत रोचक है कि हिमाचल में लोग तीन या दो सेटों में गांवों के बीच प्रवास नहीं करते। किब्बर जैसे स्थान, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, वहां लोग पूरे साल रहते हैं। नेपाल में भी मौसमी प्रवास नहीं होता, सिवाय हमारे निकटवर्ती दो गांवों—टिंकर और छांगरु—के, जो काली नदी के पार हैं। नेपाल के आगे पूर्व में, जैसे हुमला में, लोग 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी पूरे साल रहते हैं और साल भर का स्टॉक रखते हैं। उत्तराखंड में हम अकेले हैं जहां यह प्रथा है, और इसे मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र के संयुक्त अध्ययन के रूप में देखा जाना चाहिए कि तीन सेटों में गांव कैसे अस्तित्व में आए।
जोहार का भूगोल
जोहार मुख्य रूप से गोरी गंगा की घाटी है। गोरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जोहार की दक्षिण-पश्चिमी सीमा रामगंगा नदी से बनती है, जो इसे दानपुर से अलग करती है। दक्षिण में कुछ छोटी पहाड़ियां जोहार को सीरा (आधुनिक दीदीहाट, गंगोली और अस्कोट के आसपास का क्षेत्र) से अलग करती हैं। यह सीमा रेखा फिर छिपलाकोट चोटी तक जाती है, जो स्थानीय क्षेत्र में एक पवित्र स्थान है। पूर्वी सीमा पंचचूली समूह की विशाल श्रृंखलाओं से बनती है, जो इसे दरमा से अलग करती है। उत्तर में यह सीमा रेखा उंताधुरा दर्रे तक पहुंचती है। मिलम ग्लेशियर के चारों ओर घूमने के बाद, यह सीमा रेखा नंदा देवी समूह की चोटियों के साथ दक्षिण की ओर नंदा कोट चोटी तक जाती है। यहां जोहार और कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है: नंदा देवी पूर्व, या सुनंदा देवी (7,434 मीटर)। पश्चिम और उत्तर में जोहार के पास गढ़वाल का पैखंडा क्षेत्र है।
जोहार में तीन प्रमुख क्षेत्र हैं: मल्ला जोहार, गोरीफट और तल्लादेस। जलवायु और व्यापार ने शौकाओं को साल भर इन तीनों के बीच चलायमान रखा। तल्लादेस (“निचला देश”) इन चोटियों से गुजरने वाली रिजलाइन के पश्चिम में है, और कलमुनि दर्रा आपको यहां से गोरीफट तक ले जाता है। प्रसिद्ध बिरथी झरना भी यहीं है। गोरीफट गोरी गंगा की निचली घाटी है, जो आगे जाकर जौलजीबी में काली नदी से मिलती है। गोरीफट और तल्लादेस की जलवायु कुमाऊं और गढ़वाल की बाकी पहाड़ियों जैसी है। लेकिन मल्ला जोहार (“ऊपरी जोहार”), गोरी और रालम नदी के संगम के उत्तर में स्थित क्षेत्र, बहुत अलग है। हिमालय की चोटियों के पीछे होने और घाटी के तल की ऊंचाई के कारण, यहां ऊंचे पेड़ दुर्लभ हैं। घास के मैदान इनकी जगह लेते हैं, और उससे ऊपर केवल ग्लेशियर और मोरेन हैं। यह क्षेत्र साल के आधे समय बर्फ से ढका रहता है।
उत्पत्ति
इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद, जोहार के शौका साल भर मौसम के अनुसार चलायमान रहते थे। यह क्षेत्र न केवल आबाद था, बल्कि समृद्ध भी था। इसका कारण जानने के लिए हमें इतिहास की ओर देखना होगा। इस दूरस्थ क्षेत्र में सबसे पहले कौन लोग बसे होंगे? उनकी उत्पत्ति दक्षिण से हुई या वे तिब्बती थे? अधिकांश ब्रिटिश इतिहासकारों का मानना था कि भोटिया तिब्बत से आए थे। इसका कारण समझना आसान है: उनकी आंखें, भाषा, और कुछ क्षेत्रों में लिपि तिब्बती मूल की प्रतीत होती है। हां, बौद्ध धर्म तिब्बत में भारत और नेपाल से पहुंचा था, लेकिन वहां के लोग चीनी मूल के हैं, और उनकी भाषा तिब्बतो-बर्मन परिवार की है।
जोहार में एक शाक्य लामा आए थे, जो शायद साक्य बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे, और उनके शिष्यों ने इन भूमियों को बसाया। इसलिए नाम “शौका” पड़ा। हालांकि, इसके विपरीत, “शौका” शब्द “शक” जनजाति से भी उत्पन्न हो सकता है, जो कभी भारत में सबसे शक्तिशाली थी। इन्हें इंडो-स्काइथियन भी कहा जाता था। शौका शब्द और लोग कहां से आए, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। कुछ का मानना है कि शक और खस एक ही जातीय पहचान की दो लहरें थीं, जो हिमालय के विभिन्न हिस्सों में फैलीं। बाद में तिब्बती बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ लामा की कहानी भी जोड़ी गई।
बौद्ध प्रभाव और परिवर्तन
दो बातें स्पष्ट हैं: पहला, जोहार और अन्य भोट क्षेत्रों में बौद्ध धर्म कभी बहुत प्रचलित था। लेकिन पूरे हिमालय में केवल उत्तराखंड में यह बौद्ध पहचान लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है। केवल जाध लोग ही हैं, जहां यह पहचान बची है—वहां एक मठ है, और “मणि पद्मे हुम्” अभी भी गूंजता है। ब्राह्मणवादी प्रभाव और संस्कृतीकरण की प्रक्रिया इतनी मजबूत थी कि यह पहचान मिट गई। दूसरा, भोटिया क्षेत्रों में समय के साथ बदलाव आए। बाहरी लोग और समुदाय यहां आए और मिल गए। नैन सिंह रावत, तिब्बत के पहले सर्वेयरों में से एक, ऐसे ही एक बाहरी समूह, मिलमवाल या रावत, से थे।
व्यापार और जीवनशैली
मध्यकाल में जोहार में व्यापार प्रमुख गतिविधि बन गया था। शौका भारत-तिब्बत व्यापार के संरक्षक थे। वे तिब्बत से लेकर उत्तराखंड की तलहटी तक अपनी गतिविधियां चलाते थे। 1962 के भारत-चीन युद्ध ने इस व्यापार को अचानक रोक दिया। कई व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ, उनके सामान तिब्बत में फंस गए, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद यह व्यापार कभी शुरू नहीं हुआ। हिमालय के सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लोगों की हजारों साल पुरानी जीवनशैली खत्म हो गई।
जोहार के शौका, जिन्हें सोक्पा भी कहा जाता है, मूल रूप से व्यापारी थे। उनकी जिंदगी व्यापार के इर्द-गिर्द घूमती थी। आज, हालांकि व्यापार मर चुका है, कुछ लोग अभी भी मल्ला जोहार में प्रवास करते हैं, मुख्य रूप से चरवाहे के रूप में। मुनस्यारी एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन रहा है। जोहार की संस्कृति अब कुमाऊंनी संस्कृति से बहुत अलग नहीं है।